कृति ‘अंधायुग’ की रचना प्रक्रिया के बारे में भारती जी लिखते हैं …


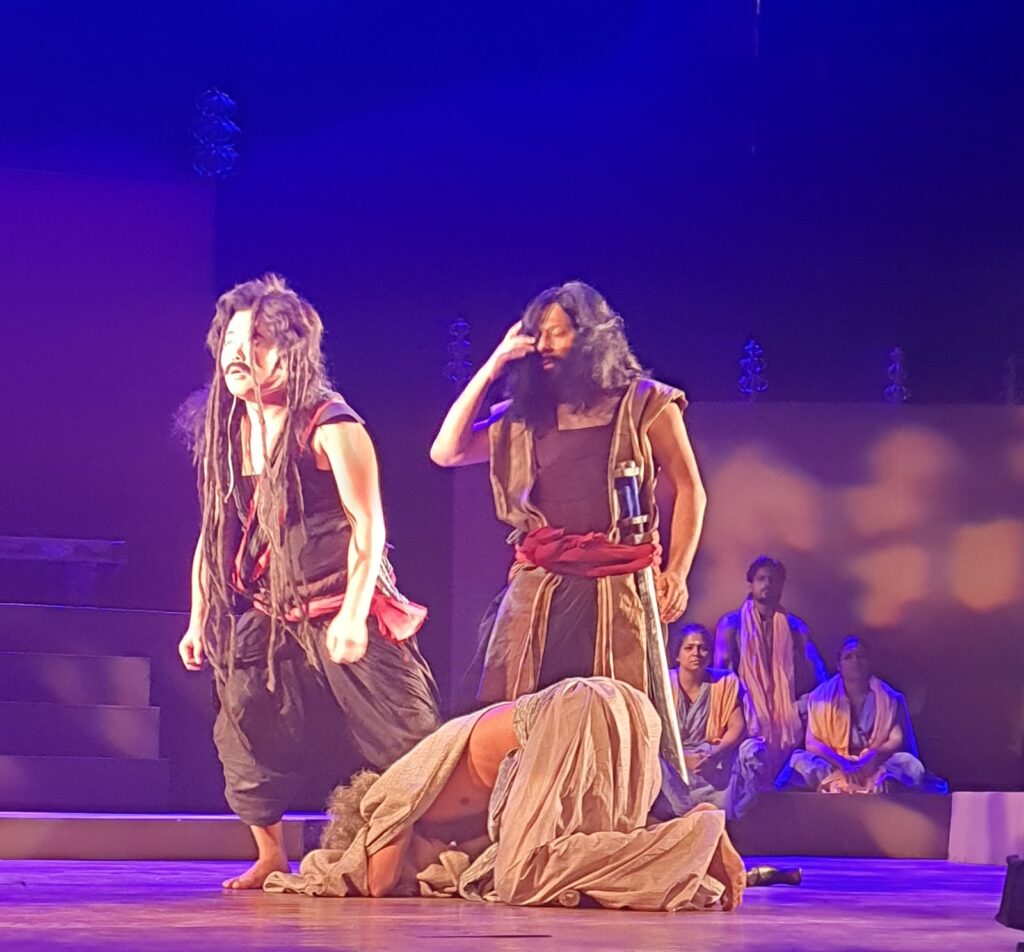



‘अन्धा युग’ कदापि न लिखा जाता, यदि उसका लिखना-न लिखना मेरे वश की बात रह गयी होती ! इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अन्तर में उभरा तो में असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा। लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रक्खा कि फिर बच कर नहीं लौटूंगा !
पर एक नशा होता है- अन्धकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डोलकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर, बचा कर, धरातल तक ले जाने का इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला-मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गयी।
एक स्थल पर आकर मने का डर छूट गया था। कुण्ठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अन्धापन- इनसे हिचकिचाना क्या इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं, तो इनमें क्यों न निडर धँसूँ ! इनमें धँस कर भी मैं मर नहीं सकता ! “हम न मरै, मरिहै संसारा !”
पर नहीं, संसार भी क्यों मरे ? मैंने जब वेदना सब की भोगी है, तो जो सत्य पाया है, वह अकेले मेरा कैसे हुआ ? एक धरातल ऐसा भी होता ‘है जहाँ ‘निजी’ और ‘व्यापक’ का बाह्य अन्तर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते। ‘कहियत भिन्न न भिन्न।’
यह तो ‘व्यापक’ सत्य है। जिसकी ‘निजी’ उपलब्धि मैंने की ही उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाये
-धर्मवीर भारती